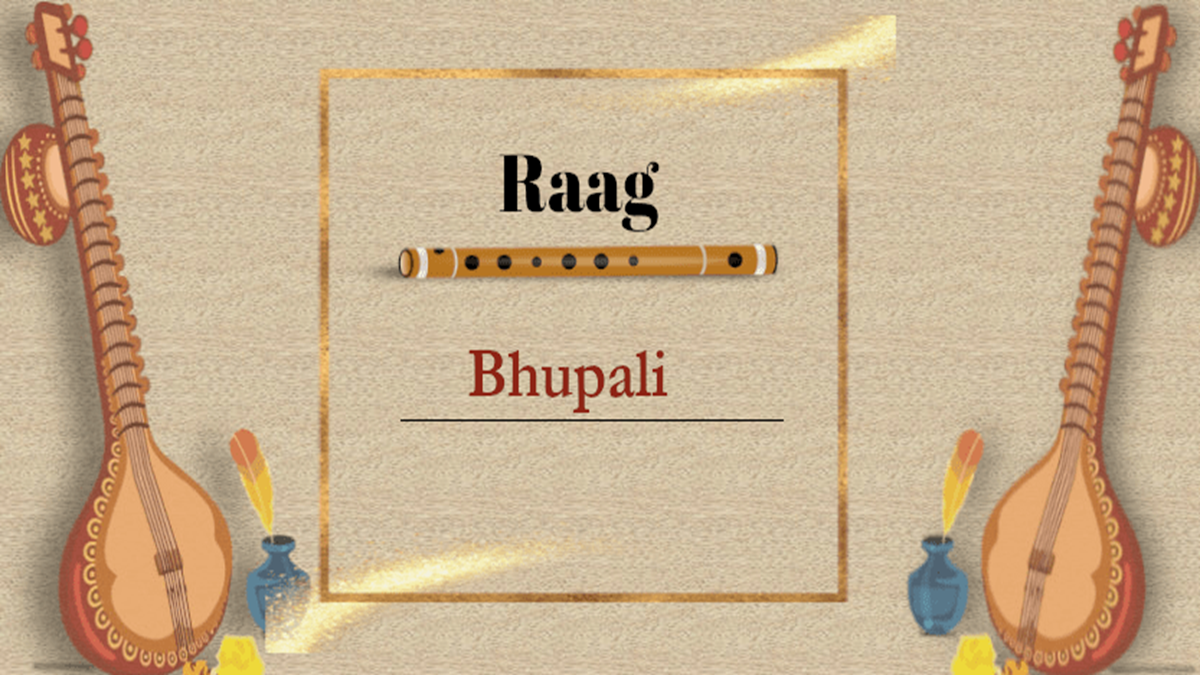The Magic Of Raga Bhupali In Film Songs | न्याज़िया बेगम: कुछ गीत हमको बरबस ही अपनी ओर नहीं खींच लेते हैं और एक अनुपम सुख की अनुभूति कराते हैं, जैसे- फिल्म सेहरा का गीत, पंख होते तो उड़ आती रे… , ज्योति कलश छलके …, फिल्म भाभी की चूड़ियां से- चंदा है तू, मेरा सूरज है तू…., फिल्म रुदाली से- दिल हूम हूम करे….., इन आंखों की मस्ती के …., फिल्म- उमराव जान, या हम तुमसे न कुछ कह पाए…., फिल्म ज़िद्दी से और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए…, फिल्म – सिलसिला से।
फिल्मी गीतों में राग भूपाली का जादू
पर आपको पता है, कि ये कुछ एक जैसे जज़्बातों का तूफान दिल में क्यों उठाते हैं? नहीं! तो हम आपको बता दें कि ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित या निबद्ध कुछ ऐसे गीत हैं जिनपर किसी राग की छाया है, जी हां ये हैं राग भूपाली पर आधारित गीत, इस राग के चलन पर कुछ और गीतों की बात करें तो फिल्म पाकीज़ा में ई बंधन बंधो …, आप शोभा गुर्टू की आवाज़ में सुन सकते हैं, मीरा फिल्म में गीत गिरधर गोपाला …, सुन सकते हैं, एम एस सुब्बुलक्ष्मी और एस वेंकट रमन के युगल स्वर में। सुर संगम फिल्म में आप लता मंगेशकर और राजन मिश्र को को सुन सकते हैं, गीत- जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी … गीत में।
ताल हैं अलग-अलग
ये सब गीत बोलों में भावों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ताल भी कहीं कहरवा है कहीं दादरा तो कहीं तीनताल। कोई भजन का एहसास दिलाता है, कोई लोरी का, कोई श्रृंगार रस का, तो कोई ठुमरी का। फिर भी एक सुकून है इनमें जानते हैं क्यों? क्योंकि भूपाली राग का गुण है, कि वो हमें शांति देता है, सुख देता है। और लोग इसे राहत के लिए बतौर थेरेपी भी यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि इसे सुनने या बजाने से हृदय गति और श्वसन क्रिया को संतुलित करने में मदद मिलती है, शायद इसलिए भी कि भक्ति और स्थिरता इसमें कूट कूटकर भरी है। इस राग को संस्कृत शब्द ‘भूप’ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राजा या स्वामी।
कर्नाटक संगीत से हुआ है विकास
भूपाली का विकास कर्नाटक संगीत में मोह लेने वाले राग यानी मोहनम रागम से माना जाता है हालांकि इसके स्वरों में थोड़ा फर्क समझ में आता है। फिर भी भूपाली और मोहनम की संरचना इसे ध्रुवपद गाने के लिए उपयुक्त बनाती हैं, क्योंकि इसके स्वर एक पंचकोणीय ढांचा बनाते हैं।
स्वर विन्यास पर नज़र डालें तो
राग भूपाली के आरोह और अवरोह दोनों में केवल पाँच स्वरों का उपयोग होता है जो सरल और सुंदर प्रतीत होती है, जिनमें म और नि को छोड़ दिया जाता है। आरोह: में बढ़ते हुए स्वर हैं – सा रे गा पा ध सा, अवरोह में – सा ध पा गा रे सा, पकड़ जो राग का थोड़ा परिचय भी दे देती है वो है- गा रे पा गा, सा ध सा रे गा, सभी स्वर शुद्ध हैं अर्थात इनमें कोई कोमल या तीव्र स्वर नहीं है, इसीलिए इसे प्राचीन रागों में शामिल जाता है।
राग भूपाली में वादी और संवादी
वादी और संवादी की बात करें तो, वादी गांधार है और संवादी धैवत है, थाट है कल्याण। तानों और अलाप में ज़्यादातर ग और ध को प्रयुक्त किया जाता है। गायन समय है, रात्रि का प्रथम प्रहर, यानि शाम 7 से रात 10 बजे तक, जाति – औडव मानी जाती है। ये थीं राग भूपाली की बातें, संगीत प्रेमियों के लिए ।