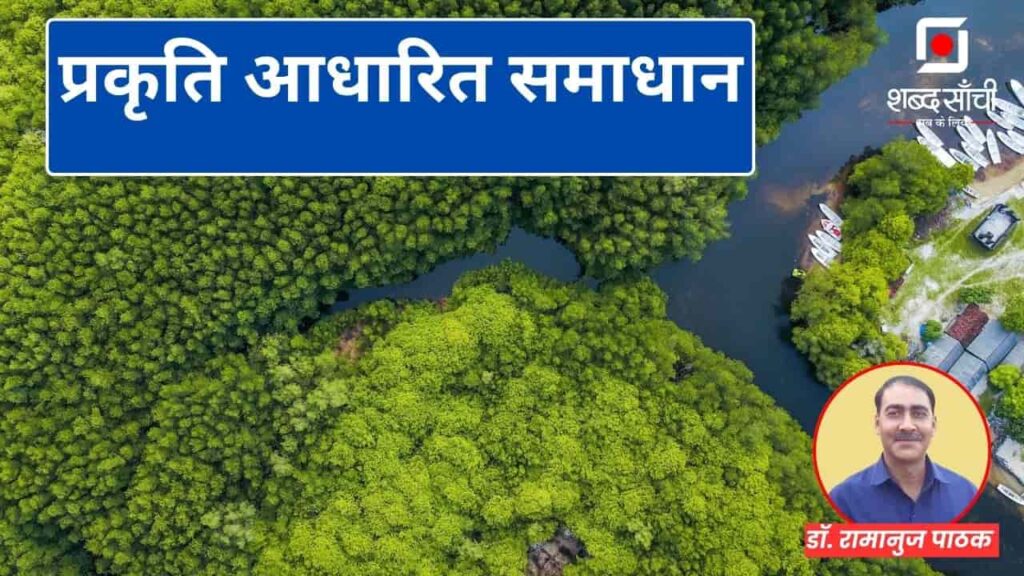Nature Based Solutions Kya Hote Hain | मानव सभ्यता की प्रगति का आधार प्रकृति रही है, परंतु यह प्रगति जब अंधाधुंध विकास और उपभोग में बदल गई, तो पारिस्थितिक संतुलन डगमगाने लगा। जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता की हानि और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती तीव्रता इसी असंतुलन का परिणाम हैं।
ऐसे में, वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि प्रकृति स्वयं संकट का समाधान भी है। “प्रकृति आधारित समाधान” (नेचर बेस्ड सॉल्यूशन- एन बी एस) अब वैश्विक जलवायु नीति, जैव विविधता रूपरेखाओं और सतत विकास की रणनीतियों में केंद्रीय स्थान पा रहा है।
वर्तमान मानव सभ्यता जिस विकास की दौड़ में आगे बढ़ रही है, उसमें पर्यावरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैव विविधता का क्षरण और पारिस्थितिक तंत्रों का विघटन एक सामान्य परिदृश्य बन चुका है।
इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ( आई पी बी ई एस)की 2019 की रपट के अनुसार, 10 लाख से अधिक प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनमें से अधिकांश आने वाले दशकों में विलुप्त हो सकती हैं यदि वर्तमान रुझान जारी रहा।
वहीं आई पी सी सी 2023 की रपट कहती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान 1850 के पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है । इसके दुष्परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात, समुद्री जलस्तर वृद्धि, जल संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याएँ दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही हैं।
Nature Based Solutions | नेचर बेस्डसॉल्यूशन- एन बी एस
ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक समुदाय अब प्रकृति आधारित समाधानों (नेचर बेस्डसॉल्यूशन- एन बी एस) को जलवायु और जैवविविधता संकट की दोहरी चुनौती का उत्तर मानता है। यह विचार वैश्विक मंचों पर मान्यता पा रहा है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी), विश्व आर्थिक मंच (डब्लू ई एफ), और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (के एम जी बी एफ), जिसमें वर्ष 2030 तक 30 फीसद भूमि और समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण का लक्ष्य है।
प्रकृति आधारित समाधानों की अवधारणा केवल पारिस्थितिकीय नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से भी सशक्त है, क्योंकि यह स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पारंपरिक ज्ञान और सतत विकास को एकजुट करती है। यह हमारे समय की एक ऐसी जैविक ढाल है, जो संकटों को मोड़ सकती है, यदि उसे विज्ञान, नीति और जनसहभागिता से सिंचित किया जाए।
प्रकृति आधारित समाधान वे उपाय हैं जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत प्रबंधन करते हुए सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। इसका लक्ष्य है मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ताकि पारिस्थितिक सेवाएँ जैसे; स्वच्छ जल, उपजाऊ मिट्टी, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु नियमन स्थायी रूप से उपलब्ध रह सकें।जानना आवश्यक है कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जैवविविधता रूपरेखा और प्रकृति आधारित समाधान क्या हैं?
दिसंबर 2022 में अपनाई गई कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जैवविविधता रूपरेखा ( के एम जी बी एफ ) रूपरेखा के लक्ष्य स्पष्ट हैं: जैसे;वर्ष 2030 तक जैवविविधता की क्षति को रोकना,30 फीसद भूभाग और समुद्री क्षेत्र का संरक्षण,पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भूमिका को सशक्त बनाना।
इस रूपरेखा में प्रकृति आधारित समाधानों को एक कुंजी के रूप में मान्यता दी गई है। यह रूपरेखा सतत विकास के 2030 एजेंडा के लक्ष्यों (एस डी जी एस) से भी गहराई से जुड़ी हुई है, विशेषकर एस डी जी एस 13 (जलवायु कार्रवाई),एस डी जी एस -15 (स्थलीय जीवन) और एस डी जी एस-16 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) से।
जलवायु संकट से निपटने में प्रकृति आधारित समाधान की भूमिका अद्वितीय है। जैसे;कार्बन शोषण और वन संरक्षण के लिए
वनों को बचाना और नये जंगल लगाना सर्वदा कारगर होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में सहायक होता है। उदाहरणस्वरूप, मैंग्रोव वनस्पति समुद्री तटीय क्षेत्रों में न केवल जैवविविधता का केंद्र हैं, बल्कि चक्रवातों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
शहरों में हरियाली बढ़ाना, छतों पर बागवानी और जलाशयों का पुनरुद्धार तापमान को नियंत्रित करने, वर्षा जल संग्रहण और बाढ़ को रोकने में सहायक होता है।शहरी हरित क्षेत्र और जल प्रबंधन से जलवायु संकट से बचाव किया जा सकता है।
पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें भी जलवायु संकट से निपटने की कारगर तरीके हैं। जैसे;
राजस्थान के ‘जोहड़’ और महाराष्ट्र के ‘पाट सिस्टम’ जैसे पारंपरिक जल स्रोत आज प्रकृति आधारित समाधान के प्रेरणास्रोत हैं। इनसे स्थानीय समुदायों की जल आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है।
प्रकृति आधारित समाधान केवल पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि आजीविका का भी आधार बन सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण और आर्थिक लाभ साथ साथ होता है।उदाहरणस्वरूप: प्राकृतिक पारिस्थितिक पर्यटन (इको-टूरिज्म )को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार में वृद्धि भी होती है।
सतत कृषि पद्धतियाँ जैसे बहुस्तरीय फसल प्रणाली मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखती हैं।
बीज बैंक और जैविक खेती स्थानीय फसलों के संरक्षण में मदद करती हैं।
हालांकि प्रकृति आधारित समाधान के लाभ अनेक हैं, लेकिन इन्हें प्रभावी बनाने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं: जैसे;अल्पकालिक आर्थिक लाभ के आगे दीर्घकालिक पारिस्थितिक निवेश की उपेक्षा होती है। परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी की कमी रहती है।निगरानी और मूल्यांकन के लिए मानक ढांचे का अभाव होता है।
यद्यपि समाधान की दिशा में अनेकानेक प्रयास भी हुए हैं। जैसे;नीति निर्माण में प्रकृति आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। शिक्षा और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को सहभागी बनाया जा रहा है। स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय किया जा रहा है। निजी क्षेत्र को हरित निवेश की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।
प्रकृति आधारित समाधान महज पर्यावरण संरक्षण की एक रणनीति नहीं, बल्कि सतत विकास के लिए एक समग्र, विज्ञान-आधारित और समुदाय-केन्द्रित दर्शन है। यह विचार अब वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माण दोनों में स्वीकार्यता पा रहा है।
उदाहरणस्वरूप:
नेचर जर्नल में प्रकाशित एक 2022 के अध्ययन के अनुसार, यदि प्रकृति आधारित समाधानों को वैश्विक स्तर पर कुशलता से लागू किया जाए तो यह वर्ष 2030 तक वार्षिक 11.3 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को घटा सकता है, जो कुल वैश्विक उत्सर्जन का लगभग एक-तिहाई है।
प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ(आई यू सी एन )2020 के अनुसार प्रकृति आधारित समाधानों से जुड़े कार्यक्रमों में निवेश से हर 1 डॉलर पर 4 से 10 डॉलर का सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त, प्रकृति आधारित समाधानों की विशेषता यह है कि यह कम लागत में बहु-क्षेत्रीय लाभ देता है, जैसे कि जलवायु शमन, आपदा प्रबंधन, रोजगार सृजन, जल संरक्षण और जैवविविधता सुरक्षा। यह उन विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो जलवायु संकट के सबसे अधिक शिकार हैं लेकिन जिनके पास तकनीकी और आर्थिक संसाधन सीमित हैं।
किन्तु, प्रकृति आधारित समाधानों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि:
इसे हरित धुलाई (ग्रीनवॉशिंग’) का साधन न बनने दिया जाए, यानि कंपनियाँ केवल दिखावटी हरियाली न फैलाएँ।स्थानीय समुदायों, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण आबादी, को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेश किया जाए।
नीति और योजना निर्माण में वैज्ञानिक मूल्यांकन, जी आई एस आधारित भू-मानचित्रण, और पारिस्थितिक सेवाओं की निगरानी को अनिवार्य किया जाए।
प्रकृति आधारित समाधान केवल पारिस्थितिकी को बहाल करने की विधि नहीं हैं, बल्कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और पारिस्थितिकीय बुद्धिमत्ता का सम्मिलन भी हैं।
वर्तमान में, वैज्ञानिक समुदाय इन समाधानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता की रक्षा करने और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय के रूप में देख रहा है। उदाहरणस्वरूप, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझा गया है, जिसमें पेड़-पौधे वनों के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और उसे दीर्घकालिक रूप से मिट्टी या जैविक संरचना में संग्रहित कर देते हैं।
शोध से यह सिद्ध हुआ है कि मैंग्रोव वन, पीट भूमि (पीट लैंडस) और समुद्री घास जैसे पारिस्थितिक तंत्र पारंपरिक वनों की तुलना में कहीं अधिक कार्बन का भंडारण करते हैं।हरी अवसंरचना जैसे कि शहरी वन, हरित छतें, वर्षा उद्यान (रैन गार्डेन्स) और जैविक जल संचयन प्रणाली, शहरी ताप द्वीप प्रभाव (अर्बन हीट आइस लैंड इफेक्ट ) को कम करते हैं।
अनुसंधान दर्शाते हैं कि ऐसे उपाय शहरी तापमान को औसतन 2–3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की मांग और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी घटता है।
इसके अतिरिक्त, जैव विविधता के संरक्षण में भी प्रकृति आधारित उपायों की भूमिका वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। विविध प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने से न केवल भोजन श्रृंखला सुदृढ़ होती है, बल्कि परागण, रोग नियंत्रण और पोषण चक्र जैसे पारिस्थितिकीय कार्य भी स्थिर रहते हैं। विश्व वन्यजीव कोष (डब्लू डब्लू एफ) और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच (आई पी बी एस )जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं ने रेखांकित किया है कि जैव विविधता का क्षरण प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है।
अंततः, प्रकृति आधारित समाधान वैज्ञानिक रूप से न केवल पर्यावरणीय संकटों का उत्तर हैं, बल्कि वे सतत विकास, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक विज्ञान-सम्मत, संवेदनशील और टिकाऊ मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं।
इसलिए, “प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास” का कथानक केवल एक पर्यावरणीय नारा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की वैज्ञानिक, नैतिक और रणनीतिक आवश्यकता है। जब हम प्रकृति को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक सहभागी मानेंगे, तभी हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जिसमें जैव विविधता और मानव विकास सह-अस्तित्व में हों।
प्रकृति आधारित समाधान केवल पारिस्थितिकी की रक्षा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और जलवायु नीति का अभिन्न हिस्सा बनने की क्षमता रखते हैं। वर्ष 2025 का कथानक “प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास” एक वैश्विक आह्वान है कि अब विकास की परिभाषा को प्रकृति के साथ पुनर्परिभाषित किया जाए। जब मानव प्रकृति के साथ नहीं, बल्कि उसमें स्वयं को समाहित करेगा, तभी वह अपने अस्तित्व को दीर्घकालिक बना सकेगा।